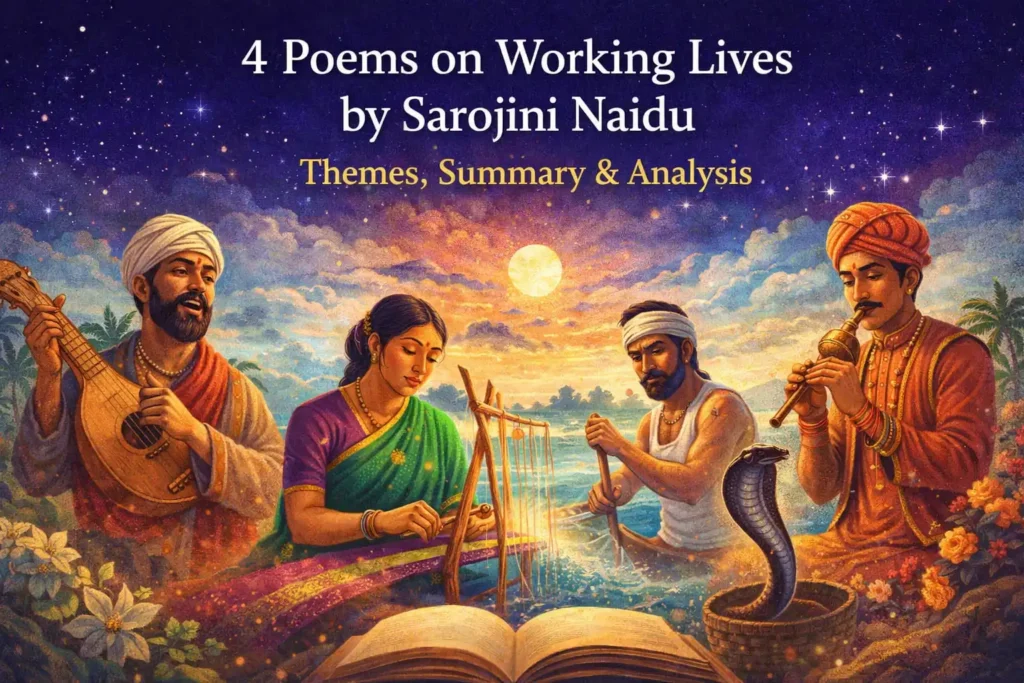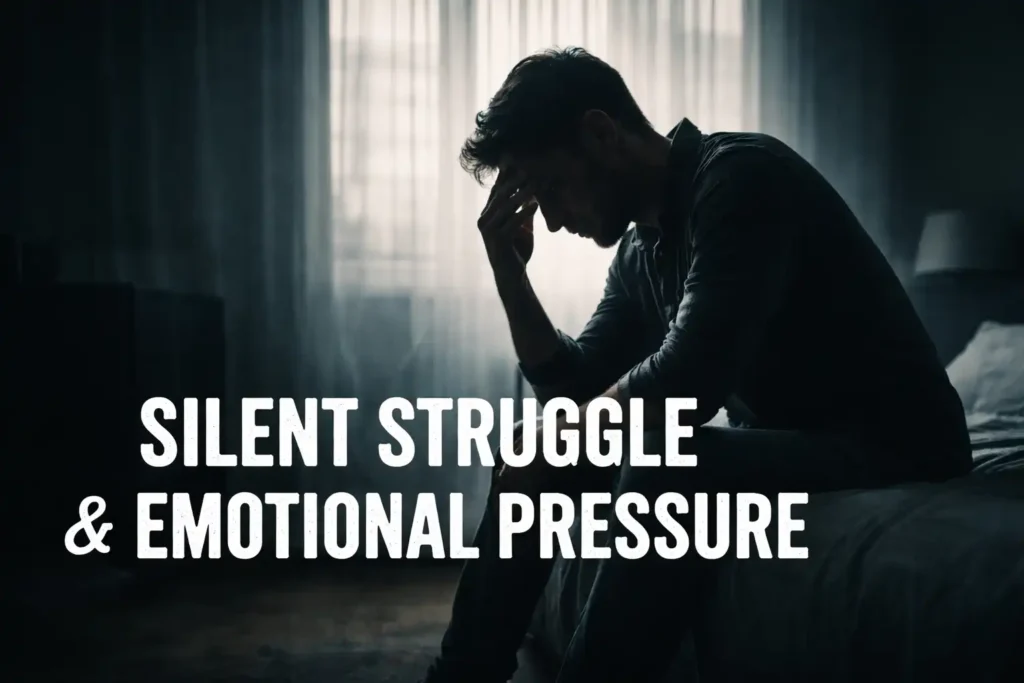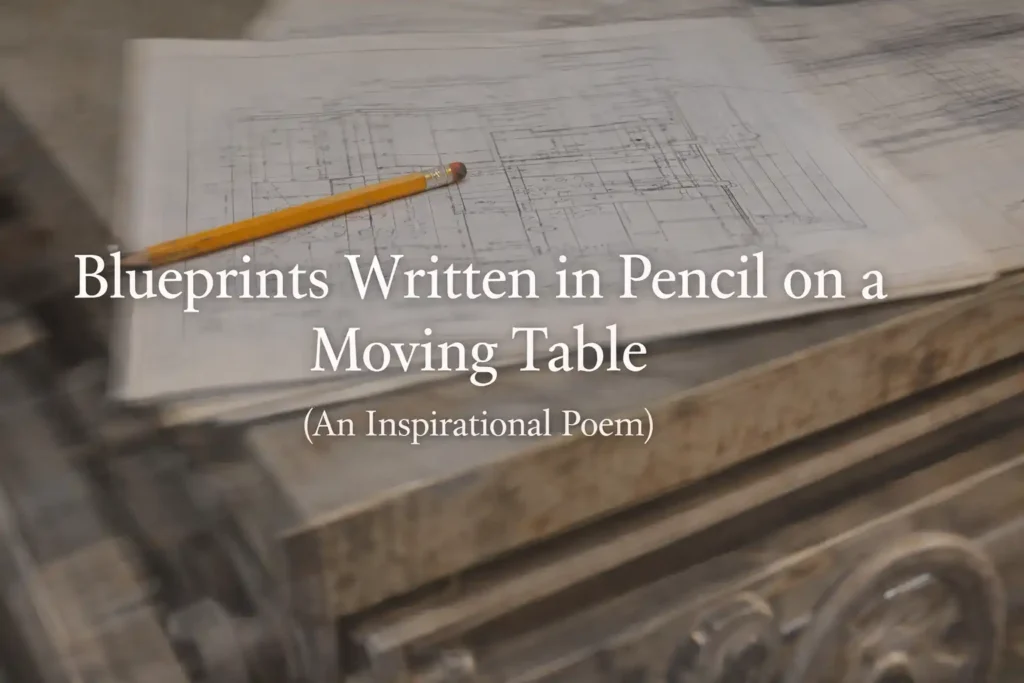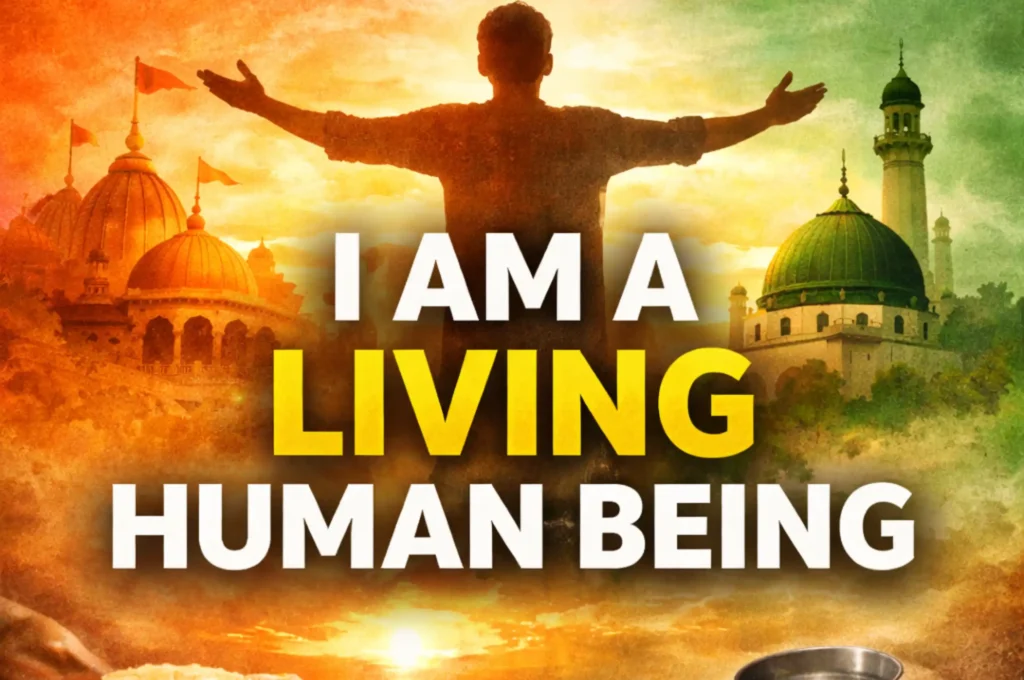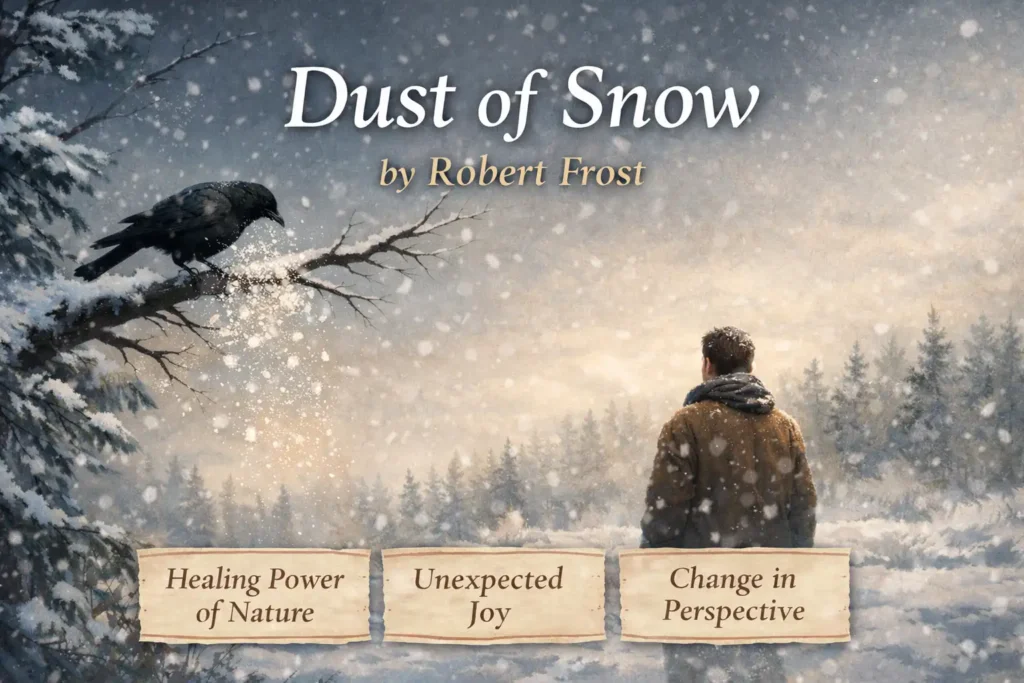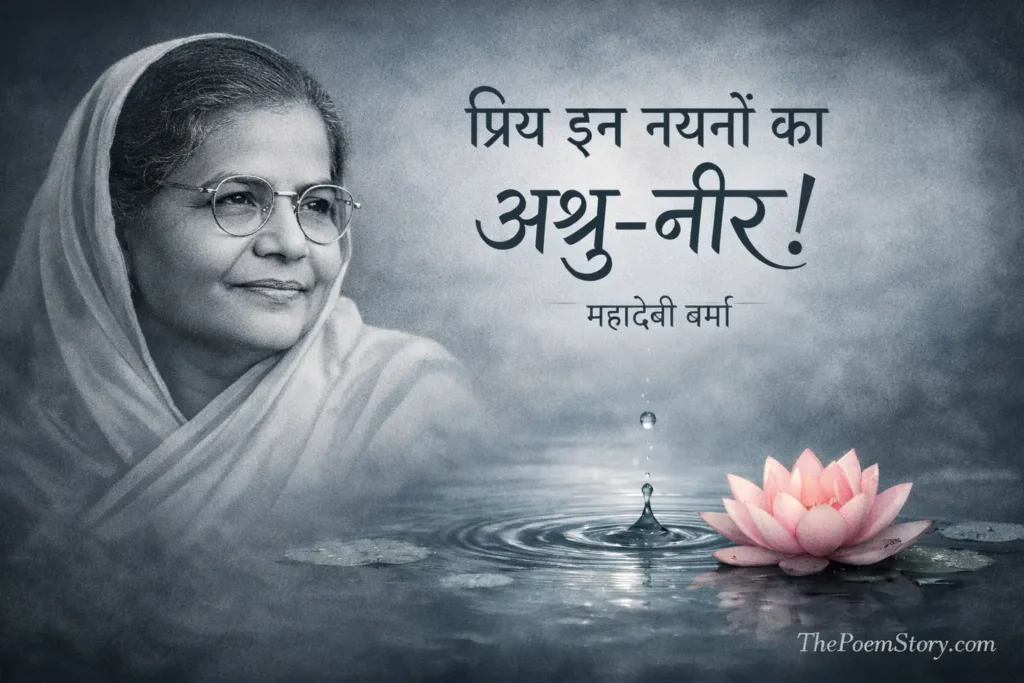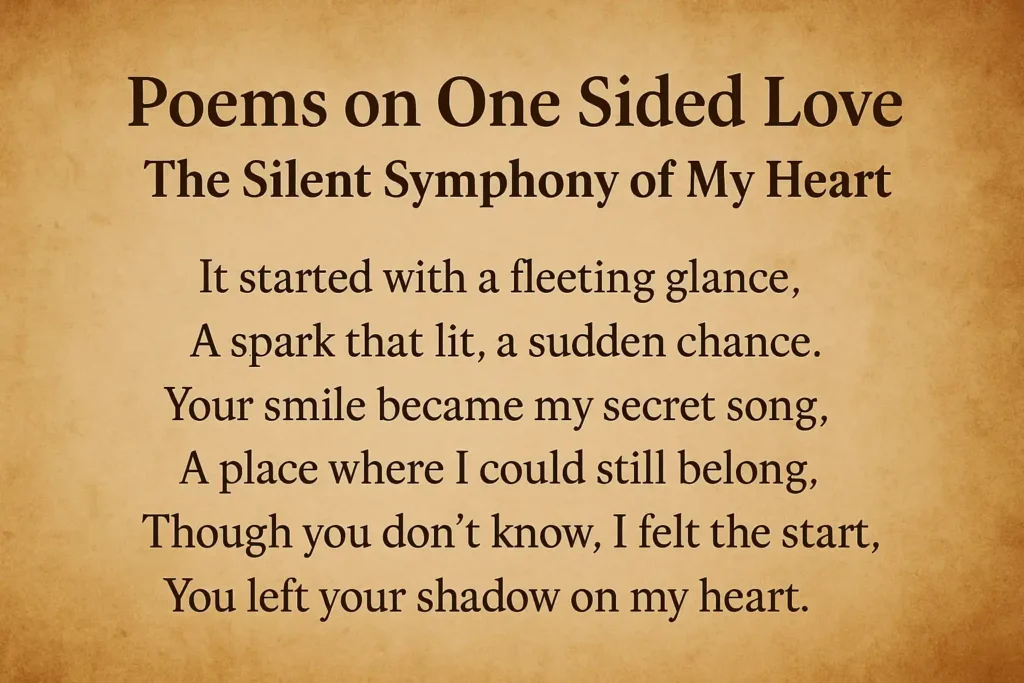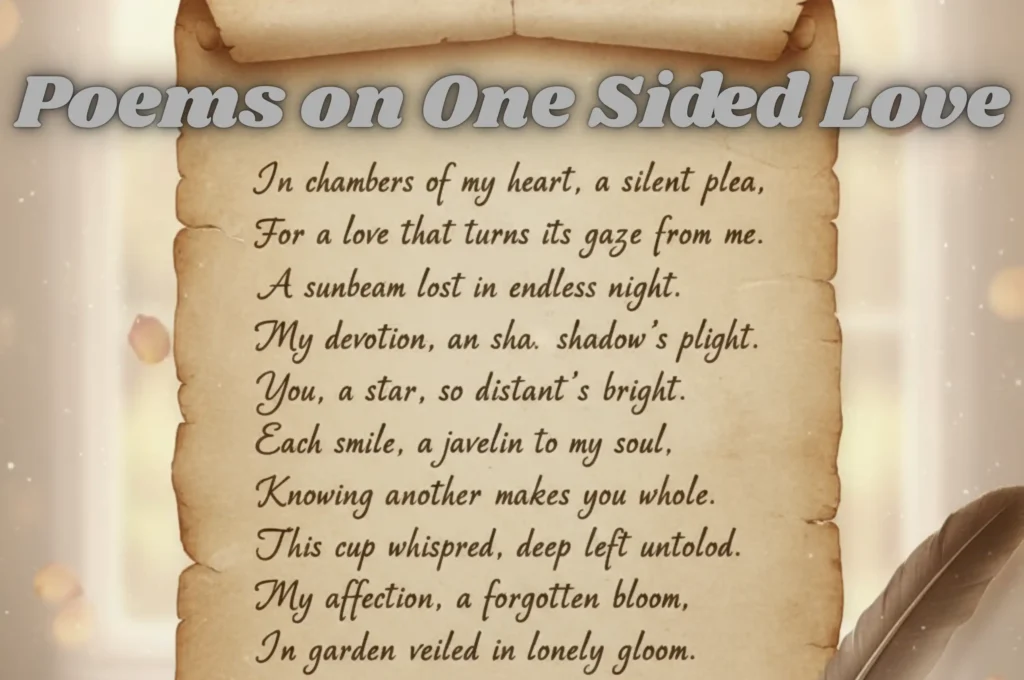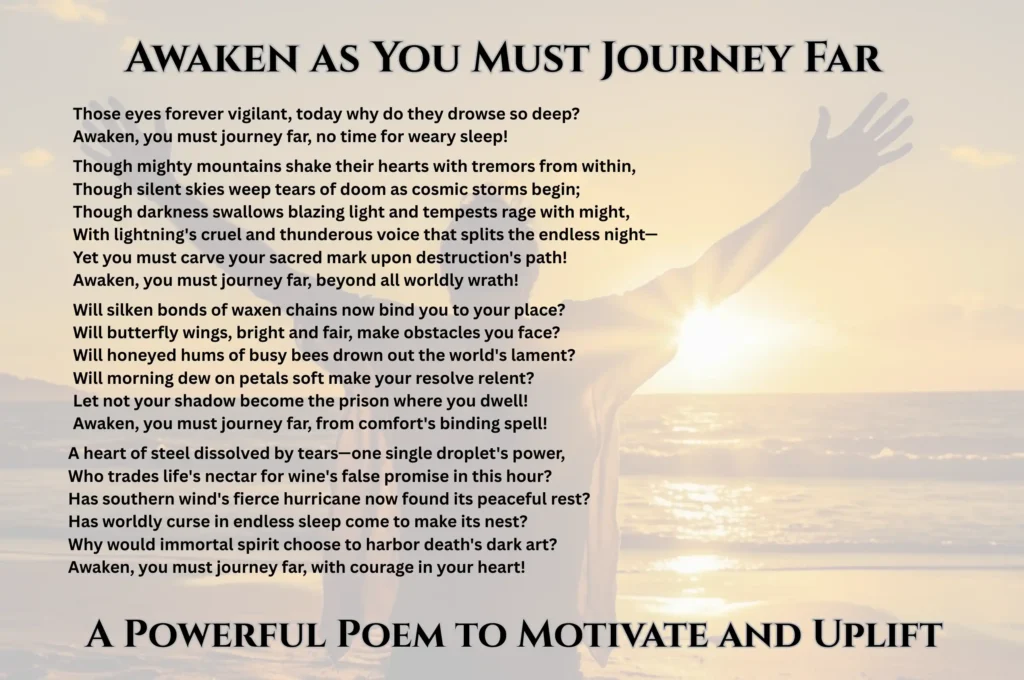कुछ पंक्तियाँ सिर्फ़ पढ़े जाने के लिए नहीं लिखी जातीं। उनका उद्देश्य सुंदर लगना या भावुक करना नहीं होता, बल्कि वे पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं। ऐसी पंक्तियाँ समाज के सामने आईना रखती हैं और उन मान्यताओं पर सवाल उठाती हैं, जिन्हें हम बिना सोचे-समझे सही मान लेते हैं। “मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ” कहना दरअसल यह याद दिलाना है कि साँस, भूख, प्यास, डर, मोहब्बत और उम्मीद—ये सब किसी धर्म के नहीं, बल्कि जीवन के गुण हैं।
यह कविता किसी धर्म, आस्था या विश्वास के विरुद्ध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना भी नहीं है। यह कविता उस संकीर्ण सोच पर प्रश्न उठाती है, जो धर्म के नाम पर इंसान को बाँट देती है। यहाँ सवाल धर्म का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का है जो इंसान को पहले हिंदू या मुसलमान बनाती है, और बाद में इंसान।
कविता एक बुनियादी लेकिन असहज प्रश्न सामने रखती है—क्या पहचान इंसानियत से बड़ी हो सकती है? क्या किसी व्यक्ति को समझने से पहले उसका नाम, रंग या धर्म जान लेना ज़रूरी है? जब भूख, प्यास, दर्द और प्रेम सबके लिए एक जैसे हैं, तो फिर विभाजन की रेखाएँ क्यों खींची जाती हैं?
भूख और प्यास जैसे साधारण उदाहरणों के माध्यम से कविता यह स्पष्ट करती है कि रंग, प्रतीक या नारे इंसानी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। ये ज़रूरतें किसी धर्म की नहीं, बल्कि एक जीवित इंसान की होती हैं। इसी सच्चाई के सामने धर्म को रंगों और पहचान तक सीमित कर देने वाली सोच खोखली प्रतीत होती है।
अंततः यह कविता हमें याद दिलाती है कि आस्था और इंसानियत एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इंसानियत को हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जब धर्म करुणा और समझ की जगह विभाजन और श्रेष्ठता का माध्यम बन जाता है, तब उस पर सवाल उठाना ज़रूरी हो जाता है। यह कविता सहमति नहीं माँगती, बल्कि आत्ममंथन की माँग करती है—कि हम पहले क्या हैं: किसी पहचान का हिस्सा, या एक ज़िंदा इंसान।
Explore more in: Poetry That Speaks to the Heart

मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ
कविता – मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ
मंदिर का हनुमान चालीसा,
मस्जिद की अज़ान हूँ।
ना हिंदू, ना मुस्लिम हूँ
मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ।मैं धर्म से पहले एक साँस हूँ
प्यार, अमन, मुहब्बत का अरमान हूँ
ना हिंदू, ना मुसलमान हूँ
मैं एक ज़िंदा इंसान हूँअगर रोश मेरी बातों पे आ जाए
अगर आहत तुम्हाती भावना हो जाए
जो काटना चाहो एक ही वार में काट देना
मत्त सवाल करना, मत्त पूछना
के हिंदू हूँ, के मुसलमान हूँ
मैं एक ज़िंदा इंसान हूँभूख लगे तो भगवा खाकर,
पेट नहीं भर पाऊँगा
गले की प्यास मैं हरे रंग से,
भी तो नहीं बुझा पाऊँगाफिर रंग पे कैसे धर्म टिका है,
इस बात से हैरान हूँ
ना मैं हिंदू, ना मुसलमान हूँ
मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ~ Nitesh Sinha (ThePoemStory)
मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ | कविता का भाव और आशय
यह कविता धर्म को नकारने या उसका अपमान करने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई है। इसमें आस्था के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन साथ ही एक ज़रूरी और ईमानदार प्रश्न भी उठाया गया है—क्या धर्म इंसान से बड़ा हो सकता है? यह प्रश्न टकराव के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के लिए है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हमने विश्वास को इंसानियत से ऊपर तो नहीं रख दिया।
कविता में हनुमान चालीसा और अज़ान को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा नहीं किया गया है। इन्हें विरोधी प्रतीकों की तरह नहीं, बल्कि समान स्तर पर रखा गया है। दोनों को एक ही साँस में शामिल करना इस बात का संकेत है कि आस्थाएँ अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य एक ही है—मानव जीवन को अर्थ, शांति और नैतिक दिशा देना। यहाँ तुलना नहीं, बल्कि समावेश की भावना दिखाई देती है।
इस संदर्भ में कविता स्पष्ट रूप से कहती है कि पहचान की शुरुआत धर्म से नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को समझने और स्वीकार करने की पहली सीढ़ी उसका इंसान होना है। धर्म, संस्कृति और परंपराएँ बाद में आती हैं। जब इंसानियत को आधार बनाया जाता है, तभी आस्था अपने वास्तविक रूप में—करुणा, सह-अस्तित्व और सम्मान के रूप में—सामने आती है।
क्या धर्म इंसान से बड़ा हो सकता है?
रंग, भूख और प्यास का प्रतीक
कविता का सबसे तीखा और सबसे ज़मीनी सवाल तब सामने आता है, जब वह रंगों को भूख और प्यास जैसी मूल मानवीय ज़रूरतों के सामने खड़ा कर देती है। यह तुलना किसी धर्म या प्रतीक का अपमान नहीं करती, बल्कि एक सच्चाई को बेहद सरल भाषा में उजागर करती है। रंग, झंडे और प्रतीक विचारों को दर्शा सकते हैं, लेकिन वे किसी इंसान की शारीरिक या भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते।
जब कविता पूछती है कि क्या भगवा रंग भूख मिटा सकता है या क्या हरा रंग प्यास बुझा सकता है, तो इसका उत्तर किसी बहस का विषय नहीं रहता। भूख भोजन से मिटती है और प्यास पानी से। इन ज़रूरतों के सामने हर प्रतीक, हर पहचान और हर वैचारिक दीवार अर्थहीन हो जाती है। यही वह बिंदु है जहाँ कविता धर्म के नाम पर खड़ी की गई सतही पहचानों पर सवाल उठाती है।
यह प्रतीकात्मक प्रश्न यह भी दिखाता है कि रंगों के आधार पर धर्म या पहचान गढ़ने की कोशिश कितनी खोखली है। अगर कोई विचार इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरतों को छू ही नहीं पाता, तो उसे इंसान से ऊपर कैसे रखा जा सकता है? भूख और प्यास किसी धर्म को नहीं लगतीं, वे केवल एक जीवित इंसान को महसूस होती हैं।
“जहाँ भूख और प्यास सवाल बन जाएँ, वहाँ पहचानें अपने आप बेमानी हो जाती हैं।”
कविता इसी सच्चाई की ओर ध्यान दिलाती है—कि इंसान को बाँटने वाली पहचानें तभी तक मज़बूत लगती हैं, जब तक हम इंसान की मूल ज़रूरतों और उसके अस्तित्व को नज़रअंदाज़ करते हैं। जैसे ही इंसान को केंद्र में रखा जाता है, रंग और लेबल अपने आप पीछे छूट जाते हैं।
मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ | यह कविता किसके लिए है?
यह कविता सबसे पहले उनके लिए है, जो हर सवाल, हर असहमति और हर पीड़ा को धर्म के चश्मे से देखने के आदी हो चुके हैं। जो किसी मुद्दे की जड़ तक जाने से पहले यह तय कर लेते हैं कि सामने वाला किस धर्म से है, और उसी आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। यह कविता उस आदत पर सवाल उठाती है, जहाँ सोच की जगह पहचान को प्राथमिकता दी जाती है।
यह कविता उनके लिए भी है, जो किसी इंसान का दर्द समझने से पहले उसका लेबल पूछते हैं। जो यह जानना ज़रूरी समझते हैं कि पीड़ित कौन है—हिंदू या मुसलमान—तभी तय करते हैं कि संवेदना दिखानी है या नहीं। कविता इस अमानवीय क्रम को उलटने की कोशिश करती है और याद दिलाती है कि दर्द का कोई धर्म नहीं होता।
इसके साथ ही, यह कविता उन लोगों के लिए भी है जो खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन भीतर ही भीतर इस बँटी हुई सोच से असहमत हैं। जो शोर का हिस्सा नहीं बनते, पर मन ही मन इंसानियत के पक्ष में खड़े रहते हैं। यह कविता उनकी चुप्पी को आवाज़ देती है और उन्हें यह भरोसा दिलाती है कि वे अकेले नहीं हैं।
यह कविता किसी को नीचा दिखाने या दोषी ठहराने के लिए नहीं लिखी गई है। इसका उद्देश्य हमला करना नहीं, बल्कि आईना दिखाना है—ताकि हम खुद से यह पूछ सकें कि हम सवालों के जवाब इंसान बनकर देते हैं या किसी पहचान के प्रतिनिधि बनकर।
अंतिम बात | मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ
अगर इस कविता से कोई आहत होता है, तो उसे केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मानकर टाल देना आसान होगा। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि हम यह समझने की कोशिश करें कि वह आहत होने की वजह क्या है। कई बार चोट शब्दों से नहीं लगती, बल्कि उस सच्चाई से लगती है, जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। जब कोई रचना हमारी जमी-जमाई धारणाओं को चुनौती देती है, तो असहजता स्वाभाविक होती है।
यह कविता किसी आस्था, स्थान या परंपरा को छोटा नहीं करती। मंदिर और मस्जिद यहाँ विरोध के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि इस बात की याद दिलाने के लिए हैं कि चाहे पूजा का तरीका अलग हो, इंसान का अस्तित्व एक ही तरह से सांस लेता है, महसूस करता है और जीता है। रंग और पहचान भी इसी तरह बाहरी परतें हैं, जो समय और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती हैं।
आख़िर में यह कविता हमें उसी मूल सत्य की ओर लौटने को कहती है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। किसी भी नाम, धर्म, रंग या पहचान से पहले हम एक जीवित इंसान हैं। अगर यह बात असहज करती है, तो शायद समस्या कविता में नहीं, बल्कि उस दूरी में है जो हमने इंसान और इंसानियत के बीच बना ली है।